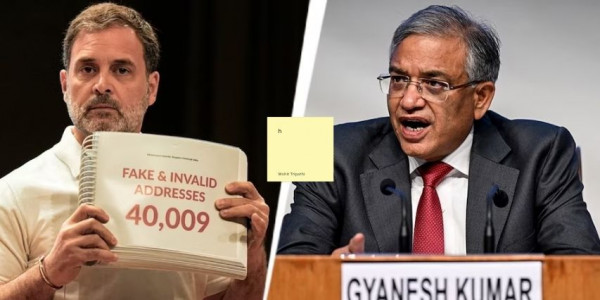इतिहास की भीड़ें लौट आई हैं, अब देखना है.. क्या जनादेश भी लौटेगा?
लखनऊ का रमाबाई अंबेडकर मैदान फिर से नीले झंडों से भरा था।
मायावती मंच पर थीं.. वही संयमित चेहरा, वही आवाज़ जो तीन दशक से यूपी की राजनीति में अपने लिए जगह बनाए हुए है। भीड़ प्रभावशाली थी, नारे गूंज रहे थे।पर सवाल वही पुराना.. क्या यह भीड़ वोट में बदलेगी?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह दृश्य नया नहीं है। 1993 से लेकर 2025 तक, बसपा की रैलियाँ हमेशा भीड़ और प्रतीकवाद का अद्भुत संगम रही हैं। कभी दलित चेतना का उत्सव, तो कभी सत्ता में हिस्सेदारी की घोषणा। लेकिन इतिहास गवाह है.. हर रैली ने उम्मीद तो जगाई, पर जनादेश सीमित ही रहा।
1993 में कांशीराम और मुलायम सिंह यादव की जोड़ी ने “मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्रीराम” का नारा दिया था। वह गठबंधन सामाजिक न्याय की नई शुरुआत थी। मगर दो साल के भीतर ही गेस्ट हाउस कांड ने उस गठबंधन को इतिहास बना दिया। इसके बाद मायावती ने सत्ता तो हासिल की, पर जनादेश कभी स्थायी नहीं बना।
2003 की लखनऊ रैली ने कांशीराम की बीमारी के दौर में बहुजन राजनीति के नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 19 सीटें ही मिलीं।
2009 आया तो बहन जी ने “दिल्ली चलो” के नारे के साथ मायावती राष्ट्रीय राजनीति में उतरने को तैयार दिखीं, मगर नतीजे रहे 20 सीटों तक सीमित। और 2014 में.. जब 2013 की बड़ी रैली के बाद पार्टी को जनाधार की उम्मीद थी.. बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी।
अब 2025 में, वही दृश्य फिर दोहराया जा रहा है। मंच वही, नारे वही, और भीड़ वही.. पर संदर्भ बदल गया है। आज का युवा मतदाता उस दौर से नहीं जुड़ा, जहाँ बहुजन आंदोलन भावनाओं से चलता था। अब पहचान की राजनीति जगह बदल चुकी है.. दलित अस्मिता के साथ अब सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक अवसरों की मांग जुड़ गई है।
बसपा के लिए असली चुनौती यही है क्या वह फिर से 90 के दशक की तरह “प्रतिरोध की राजनीति” को “प्रस्ताव की राजनीति” में बदल पाएगी? क्योंकि इतिहास बताता है.. भीड़ केवल आंदोलन की निशानी होती है, जनादेश उसकी परिणति।
आज लखनऊ की भीड़ एक संकेत है कि
2003 की लखनऊ रैली ने कांशीराम की बीमारी के दौर में बहुजन राजनीति के नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 19 सीटें ही मिलीं।
2009 आया तो बहन जी ने “दिल्ली चलो” के नारे के साथ मायावती राष्ट्रीय राजनीति में उतरने को तैयार दिखीं, मगर नतीजे रहे 20 सीटों तक सीमित। और 2014 में.. जब 2013 की बड़ी रैली के बाद पार्टी को जनाधार की उम्मीद थी.. बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी।
अब 2025 में, वही दृश्य फिर दोहराया जा रहा है। मंच वही, नारे वही, और भीड़ वही.. पर संदर्भ बदल गया है। आज का युवा मतदाता उस दौर से नहीं जुड़ा, जहाँ बहुजन आंदोलन भावनाओं से चलता था। अब पहचान की राजनीति जगह बदल चुकी है.. दलित अस्मिता के साथ अब सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक अवसरों की मांग जुड़ गई है।
बसपा के लिए असली चुनौती यही है क्या वह फिर से 90 के दशक की तरह “प्रतिरोध की राजनीति” को “प्रस्ताव की राजनीति” में बदल पाएगी? क्योंकि इतिहास बताता है.. भीड़ केवल आंदोलन की निशानी होती है, जनादेश उसकी परिणति।
आज लखनऊ की भीड़ एक संकेत है कि
नीला रंग अभी मिटा नहीं,
लेकिन अगर उसे सत्ता के नक्शे पर लौटना है,
तो पुरानी भाषा नहीं, नया विमर्श चाहिए।
For all the political updates download our Molitics App :
Click here to Download